गंभीर संकट का कामचलाऊ समाधान,
- Posted By: Tejyug News LIVE

- देश
- Updated: 28 December, 2024 07:39
- 437

गंभीर संकट का कामचलाऊ समाधान, दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब
वह तो भला हो प्रकृति का कि दिसंबर के अंतिम दिनों को दिल्ली-एनसीआर में थोड़ी सी बरसात हो गई, वरना राजधानी क्षेत्र की कोई चार करोड़ आबादी लगभग जहर को सांसों के जरिये अपने शरीर में उतार रही थी। इससे पहले ग्रेप की कई पाबंदियां लागू होने के बावजूद दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) साढ़े चार सौ के पार था। अभी न शहर में ट्रक आ रहे, न निर्माण कार्य चल रहा, न हरियाणा-पंजाब में पराली जल रही, न ही कहीं आतिशबाजी हो रही है। इसके बावजूद दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर श्रेणी में होना दर्शाता है कि सरकार में बैठे लोग या तो वायु प्रदूषण के असल मर्ज को पकड़ नहीं पा रहे या फिर कोई ईमानदारी से इसका निदान नहीं चाहता।
दिल्ली-एनसीआर के अधिकतर इलाकों में एक्यूआइ लेवल करीब 300 है। इस बार तो ठंड शुरू होने से बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने वायु को जहर होने से रोकने की कार्य योजना मांगी थी। अफसोस कि सरकार में बैठे लोग इंसान से उपजी दिक्कतों का हल मशीनों में खोजने का असफल प्रयोग करते रहे, जबकि जहरीली हवा यहां के लोगों की जिंदगी के साल काम कर रही है। वह छोटे बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रही है। इससे समाज और सरकार, दोनों पर भारी आर्थिक नुकसान की भी मार पड़ रही है।
जब दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई पा जा रही, तब यह सहज ही समझा जा सकता है कि शेष उत्तर भारत में प्रदूषण रोकने के लिए कुछ ठोस नहीं किया जा रहा होगा। दिल्ली जैसे महानगरों की त्रासदी है कि वे किसी भी समस्या के लिए पड़ोसी को दोषी बताने को तत्पर रहते हैं और अपनी आदतों एवं प्रकृति-हंता कृत्यों को कभी मजबूरी तो कभी हक के साथ स्वीकार नहीं करते। यह बात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फिर से कही है कि दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य स्रोत वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है, जिसका अति सूक्ष्म कण (पीएम) 2.5 में भागीदारी 18.8 प्रतिशत है।
दुर्भाग्य यह है कि सभी जानते हैं कि दिल्ली की हवा को खराब करने में सबसे बड़ी भूमिका वाहनों से निकले धुएं और खासकर सड़कों पर लगने वाले जाम की है, लेकिन समूचा तंत्र इस विषय में पूरी तरह गैर संवेदनशील है। इसके बावजूद वाहनों के परिचालन में सख्ती के लिए न निवासी तैयार हैं, न वाहन बेचने एवं कर्ज देने वाली वित्तीय संस्थाएं और न ही पेट्रोल-डीजल बेचने वाली लाबी। वाहनों के उत्सर्जन में नाइट्रोजन आक्साइड गैस भी होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण गंभीर होता जाता है। हमें समझना होगा कि वाहन चलने से केवल ईंधन उत्सर्जन ही हवा को जहर नहीं बनाता, बल्कि वाहन में लगी बैटरी से निकलने वाले अम्लीय अदृश्य धुएं और टायरों के सड़क से घर्षण से उत्पन्न बहुत बारीक रबर कण भी कम जानलेवा नहीं होते।
पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने दफ्तर और स्कूल के समय में बदलाव करने का प्रयोग किया था, लेकिन वह अंतराल महज आधे घंटे का था, लिहाजा उसका कोई असर परिवहन पर नहीं पड़ा। कई बार तो लगता है कि सरकार में बैठे लोग इंसानों की जान बचाने से अधिक अदालतों के सामने अपनी खाल बचाने के लिए गैरजरूरी प्रयोग कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान लेते हैं। वायुमंडलीय और मौसम की स्थितियां वायु में प्रदूषण के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालती हैं। हवा की गुणवत्ता खराब होने के दो ही बड़े कारण हैं-हाइड्रोकार्बन और धूल। हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन या तो औद्योगिक गतिविधियों से होता है या फिर आटोमोबाइल के धुएं से।
पक्की सड़कों वाले शहर में धूल कण का आगम भी यातायात की हलचल ही है। थोड़ा मौसम नम हुआ, ओस गिरी तो यही दोनों प्रदूषकों का संयोजन अक्सर स्माग पैदा कर देता है और वही जानलेवा होता है। जब तापमान गिरता है और ठंडी हवा जमीन को ढक लेती है, तो किसी भी गर्म हवा को इसके ऊपर से गुजरना पड़ता है। इस तरह प्रदूषक कण घनी ठंडी हवा में कहीं फैल नहीं पाते हैं। इस प्रकार धूल और जहरीले कणों वाली हवा पूरे परिवेश को ढक लेती है। चूंकि ठंडी हवा अधिक घनी होती है और धीमी गति से बहती है, इसीलिए दूषित हवा के हमारी सांसों में बस जाने और उसके गंभीर परिणाम होने की आशंका ठंड और ओस के दिनों में सर्वाधिक होती है। यदि विज्ञान के इसी सिद्धांत के मुताबिक दिल्ली में सतर्कता बरती जाए और प्रदूषण नियंत्रण की योजना बने तो इस संकट को काफी कुछ कम किया जा सकता है।
सड़कों पर भीड़ कम करने के लिए खराब वाहनों को सड़क पर आने से रोकने जैसे तात्कालिक उपाय तो ठीक हैं, लेकिन इसके लिए कुछ दूरगामी उपाय भी करने होंगे, जैसे गैरजरूरी कार्यालयों को दिल्ली-एनसीआर से दूर भेजना होगा। बस स्टैंड की मौजूदा व्यवस्था में सुधार और रिंग रेलवे को मजबूत करना होगा। अलग-अलग सड़कों पर विभिन्न गति वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगानी होगी। आवासीय इलाकों में बाजार बनाने से रोकना होगा। साथ ही गंभीर दिनों में हर तरह के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि आयोजनों पर रोक लगानी होगा, जो सड़क घेरते हों या जाम पैदा करते हैं।
पंकज चतुर्वेदी।
(लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं)

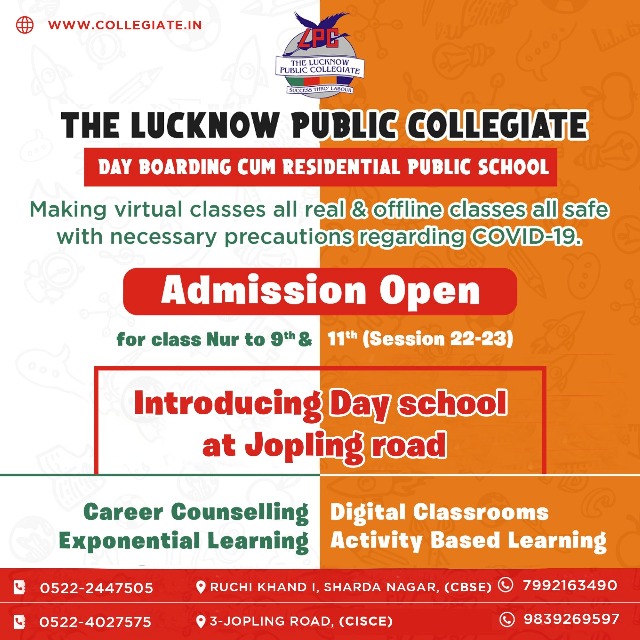





Comments